वृद्धावस्था और अकेलापन – जिम्मेदार कौन, एक पड़ताल लाइव डिस्कशन send to delhi press by mail 26/01/2017 स्वीकृत
द्धावस्था और अकेलापन – जिम्मेदार कौन, एक पड़ताल
लाइव डिस्कशन
(व्हाट्स एप ग्रुप में एक
खबर पर हुई डिस्कशन पर आधारित. सर जी के निर्देश पर तैयार की गयी)
चाय के साथ अखबार पढना मेरी दिनचर्या की प्रथम
गतिविधि होती है. वह भी मैं पहले खेल समाचारों से शुरुआत करती हूँ क्यूंकि अंत में
प्रथम पृष्ठ की नकारात्मकता और विकृत सच्चाइयों से रूबरू होना ही होता है. आज सुबह
खेल समाचार पढ़ते हुए मैंने आखिरी पन्ने पर जैसे ही नज़र दौड़ाई तो एक समाचार पढ़ कर
मन ख़राब हो गया. खबर ही कुछ ऐसी थी,
“रिटायर्ड निर्देशक का शव
बेटे का बाट जोहता रह गया”.
एक समय महत्वपूर्ण पद पर
आसीन व्यक्ति, जिसकी पत्नी मर चुकी थी एक वृद्धाश्रम में रह रहा था. उनका एकमात्र
बेटा विदेश में जा बसा था. जिसे खबर ही एक दिन के बाद मिल सकी और जिसने तुरंत आने
में असमर्थता जाहिर किया. देश में बसे रिश्तेदारों ने भी मुखाग्नि देने से इनकार
कर दिया. आश्रम के सरंक्षक ने मुखाग्नि दिया. एक समय पैसा पॉवर और पद के मद में
जीता हुआ व्यक्ति अंतिम दिनों में वृद्धाश्रम में अजनबियों के बीच रहा और अनाथों
सा मरा.
आखिर हम कहाँ जा रहें हैं? बेटे की निष्ठुरता,
रिश्तेदारों की अवहेलना ने सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर जीवन का गणित कहाँ गलत
हुआ जो अंत ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा. दुनिया में खुद के संतान होने के बावजूद
अकेलेपन का अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा. जवानी तो व्यक्ति अपनी शारीरिक
बल और व्यस्तता में बीता लेता है पर बुढ़ापे की निर्बलता और अकेलापन उसे किसी सहारे
के लिए उत्कंठित करती है. विदेशों से इतर हमारे देश में सामाजिक सरंचना ही कुछ ऐसी
है कि परिवार में सब एक दुसरे से गुथे हुए से रहतें हैं. माँ-बाप अपने बच्चों की
देख भाल उनके बच्चे हो जाने तक करतें हैं. अचानक इस ढांचें में चरमराहट की आहट
सुनी जाने लगी है. संस्कार के रूप में चले आने वाले व्यवहार में तब्दीलियाँ आने
लगी हैं. बच्चों के लिए सम्पूर्ण जीवन होम करने वाले जीवन के अंतिम वर्ष क्यूँ
अभिशप्त अकेलेपन और बेचारगी में जीने को मजबूर हो जातें हैं? इस बात की चर्चा मैंने देश भर की अलग अलग
प्रान्तों की महिलाओं से किया. सभी ने पुत्र के व्यवहार पर आश्चर्य व्यक्त किया.
अहमदाबाद की मिनी सिंह ने
छूटते ही कहा कि अच्छा है कि उनके कोई कोई बेटा नहीं है, कम से कम कोई आस तो नहीं
रहेगी. पटना की रेनू श्रीवास्तव ने कहा कि यदि बेटी होती तो शायद ये दिन देखने को
नहीं मिलते. बेटे की तुलना में बेटियाँ संवेदनशील जो होती हैं. वहीँ रानी
श्रीवास्तव ने इस बात को नकारते हुए कहा कि बात लड़का या लड़की का नहीं बल्कि समस्या
परिवेश और परवरिश का है. समस्या की जड़ में भौतिकवाद और स्वार्थीपन है.
मुंबई की पूनम अहमद ने माना कि बहुत सारी बेटियाँ
भी केयरलेस और स्वार्थी होती हैं वहीँ कई बहुएं सास के लिए सबसे बढ़ कर होती हैं.
अपनी अंतरजातीय विवाह का उदाहरण देते हुए वे कहतीं हैं कि उनकी सास और उनका रिश्ता
बहुत ही खास है. बीमार होने पर उनकी सास उनके पास ही रहना पसंद करतीं हैं और पूनम
अहमद के एक एक्सीडेंट के बाद उनकी सास ने ही सबसे ज्यादा उनका ध्यान रखा. उनका
कहना है कि पेरेंट्स को प्यार और सम्मान देना बच्चों का फ़र्ज़ है चाहे वे लड़के के
हो या फिर लड़की के.
सही बात है बात बेटा या बेटी से हट, सोच के बीजारोपण में है.
हम बच्चों को शुरू से जीवन के चूहा दौड़ में शामिल होने के लिए यही मन्त्र बातों
में पिछड़ जातें हैं. किताबी ज्ञान भले ही बढ़ते जाता है पर रिश्तों की डोर थामे
रखने की कला में अधकचरें रह जातें हैं.
सरिता पंथी जी पूछती हैं कि बच्चों को इस दौड़
में कौन धकेलता है? उनके माँ-बाप ही न, फिर बच्चों का क्या दोष? रेणु श्रीवास्तव
जी सटीक कहती हैं कि भौतिक सुखों के चाह में माता-पिता भी तो बच्चों को अकेलापन
देतें हैं उसके बचपन में, तो संस्कार भी तो वही रहेगा, वे कटाक्ष करतीं हैं कि रोपे
पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से होय. इस पर मुंबई की पूनम अहमद जी कहती हैं कि इसी से
क्रेच और ओल्ड age होम दोनों की संख्याओं में इजाफा हो रहा है.
अजमेर
में रहने वाली लीना खत्री कहतीं हैं, “हमें अक्सर बच्चों की बातें सुनने का वक़्त
नहीं होता है. यही चीज हमारे बूढ़े हो जाने पर होती है जब बच्चें जिन्दगी की आप
धापी में उलझ जातें हैं और उनके पास हमारे लिए वक़्त नहीं होता है”.
नीतू मुकुल जी कहती हैं,
“उक्त घटना ह्रदय विदारक और
चिंतनीय है. मेरे हिसाब से इस समाचार का एक पक्षीय अवलोकन करना सही नहीं. हम
बच्चों को पढ़ानें में तो खूब पैसा खर्च करतें हैं पर क्या कभी समय खर्च करने का
सोचते हैं. केवल अच्छा स्कूल और सुविधाएँ देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं”.
इंदौर की पूनम पाठक जी कहती
हैं, “ मशीनों के साथ पलता बच्चा मशीन में तब्दील हो गया है. जिसके पास संवेदनाएं
नहीं होती हैं, होता है तो सिर्फ आगे बढ़ने का जूनून, पैसा, पॉवर और सफलता पाने की जिद्द, जिसके लिए वो सभी संबंधों की
बलि देने को तैयार रहता है”.
पटना की रेणु जी अपनी चिर
परिचित अंदाज में कहतीं हैं कि ये घटना आधुनिक सभ्यता की देन है जहाँ ह्रदय संवेदन
शून्य हो कर मरुभूमि बनता जा रहा है.
इन सभी की बातें गौर फरमाने के काबिल है.
बच्चों के साथ बातें करना वक़्त गुजरना हमें उनके मानस और ह्रदय से जोड़े रखता है. दिल
और मानस को वार्तालाप के पुल जोड़तें हैं और उस वक़्त हम अपनी भावों और संस्कारों को
उनमें प्रति रोपित करतें हैं. सिर्फ अंधी दौड़ में भागना सीखाने की जगह बच्चों को
रिश्तों और जिम्मेदारियों का भी बचपन से ही बोध कराना आवश्यक है. बड़े हो कर खुद ब
खुद सीख जायेंगे ऐसा सोचना गलत है, पक्के घड़े पर कहीं मिटटी चढ़ती है भला?
बच्चें तो माता-पिता के व्यवहार का आईना होतें
हैं. कई दंपत्ति अपने बुजुर्गों के प्रति बेरुखी का भाव रखतें हैं. उनके लिए
बुड्डे-बुढ़िया या बोझ जैसे अपशब्दों का प्रयोग करतें हैं. अपनी पिछली पीढ़ी के
प्रति असंवेदनशील और लापरवाह दंपत्ति अपनी संतानों को इसी बेरुखी, संवेदनहीनता और
कर्तव्यहीनता की थाती संस्कारों के रूप में सौंपते है. फिर जब खुद बुढ़ापे की दहलीज
पर आतें हैं तो बेचारगी और लाचारी का चोला पहन अपने बच्चों से अपने पालन – पोषण के
रिटर्न की अपेक्षा करने लगतें हैं. हर बूढ़ा व्यक्ति इतना भी दूध का धुला नहीं
होता है.
मिनी सिंह पूछती हैं, “क्या माँ बाप, अपने बच्चे के परवरिश में भूल कर सकते हैं तो फिर बच्चों से कैसे भूल हो जाती
हैं?
इस पर रायपुर की दीपान्विता
राय बनर्जी बिलकुल सही कहतीं हैं,
“जिंदगी की आपाधापी में निश्चित ही हर बार
हम तराजू में तौल कर बच्चों के सामने खुद को नही रख पाते। इंसानी दिमाग गलतियों का
पिटारा ज्यादा होता है और सुधारों का गणित कम। एक तो यह कारण जो बच्चों को भी अपनी
जरूरतों के अनुसार ढलने को मजबूर कर देता है। जो माता पिता अपनी जिंदगी भरपूर जीते हैं और बच्चों से उनकी देखभाल की पूरी
उम्मीद लगाये बैठते हैं, अपने रिश्ते नातों में स्वार्थ एवं
भौतिकता को तवज्जो देते हैं, अक्सर उनके बच्चों में भी कर्तव्य बोध कम
होने के आसार होते ही हैं”.
शन्नो श्रीवास्तव जी
ने अपने अनुभवों को सुनाते हुए बताया कि उन्होंने अपने ससुर की अंतिम समय में अथक
सेवा की जिसे डॉक्टरों और सभी रिश्तेदारों ने भी सराहा. इसका कारण वे बताती है कि,
“ पहला मेरे माता पिता द्वारा दी गयी शिक्षा और संस्कार और दूसरा अपने सास-ससुर से
मिला अपनापन”.
कितना सही है ना, जिस घर में बच्चें अपने दादा
दादी, नाना-नानी को इज्जत और स्नेह सिंचित होते देखतें हैं कल को हज़ार व्यस्तताओं
के बीच अपने बुजुर्गों के प्रति फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों को वे अवश्य निभायेंगें
क्यूंकि ये बोध हर साँस के साथ उनके भीतर पल्लवित होते रहेगा.
सच ऐसा क्यूँ हो जाता है कि भरे पूरे संसार में
कोई अनाथों सा मर जाता है? जो सम्पन्न और निराश्रित भी है. अवश्य इसमें जीवन के
पूर्वार्ध के व्यवहार और रिश्तों को निभाने के गुण-अवगुण प्रमुख कारक हैं. अवश्य
ही उसने कोई ऐसा दुर्व्यवहार या अहंकार लिप्त भाव रखें होंगे जो उसकी मृत्यु के
पश्चात् रिश्तेदारों ने भी मुखाग्नि देने से इंकार कर दिया.
पूनम पाठक जी फिर
कहती हैं, “बात फिर घूमफिर वहीं आती है। उचित शिक्षा और संस्कार बच्चों के बेहतर
भविष्य का निर्माण तो करते ही हैं साथ ही रिश्तों के महत्व से भी हमे परिचित कराते
हैं। अत: सही संस्कार से बेहतर भविष्य व् रिश्तों के बीच संवेदन शीलता बनी रहती
है”.
सुधा कसेरा जी बड़े ही
स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, “हमें स्कूली पढ़ाई से अधिक
रिश्तों के विद्यालय में उन्हें पढ़ाने में यकीन करना चाहिए.
रिश्तों के विद्यालय
में यह पढ़ाया जाता है कि बच्चों के लिए उनके माता- पिता ही संसार में सबसे महान और उनके सबसे अच्छे मित्र होते हैं, दरअसल रिश्तों को लेकर हमें बहुत स्पष्ट होना
चाहिए । तथा कथित अंग्रेज़ी सीखने पर ज़ोर देने वाले विद्यालय ने बच्चे को सब कुछ पढ़ा दिया, पर रिश्तों का अर्थ नहीं पढ़ा पाए। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे , विदेश में नौकरी तो पा लेते हैं और वे विदेश में सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले माता- पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अनदेखा
करने में नहीं चूकते रिटायर्ड बाप और माँ किस काम के? विदेश की चमकीली ज़िंदगी में टूटे दांतों
वाला बूढ़ा बाप बेटे के लिए डस्टबिन से अधिक कुछ नहीं रह जाता”.
सरिता पंथी जी कहतीं
हैं, “आज के समय में मैं खुद अपने दोनों बच्चों को बाहर भेज रही हूँ इसी महीने आगे
पढ़ने. अगर उसके बाद मैं ये आस रखूं कि मेरी जरूरत के समय वापस आ जायेंगे तो ये मेरी
बेवकूफी होगी। हमें उन्हें खुला आकाश देना है तो खुद की सोच में भी परिवर्तन लाना
ही होगा”.
पद्मा अगरवाल जी का कहना है,”
मेरे विचार से बच्चों को दोषी करार देने
के पहले उनकी परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है एक ओर विदेश का लुभावना
पैकेज दूसरी ओर पैरंट्स के प्रति उनका कर्तव्य कई बार वह चाहे कर भी नहीं कर पाते. अपने कैरियर और अपनी जिंदगी के लिए भी तो उनकी कुछ चाहत और लक्ष्य होते हैं”.
हैदराबाद की सुधा
कसेरा जी का सोचना है, “सीमा तय करना हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है, जिस प्रकार माता- पिता अपने बच्चे के भविष्य निर्माण के कारण अपने सुख-
संसाधनों का परित्याग
करते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी उनके लिए अपने कैरियर से भी समझौता करना चाहिए, नौकरी विदेश में अधिक
पॅकेज वाली मिलेगी, लेकिन भारत में नौकरी मिलेगी, थोड़े पैसे कम मिल जाएंगे, इतना ही बस अंतर है.
अधिकतर जो लोग
रिश्तों को महत्व नहीं देते, वे ही विदेश में बसना पसंद करते हैं. वे यह नहीं सोचते उनके बच्चे भी बड़े
होकर उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनको कैसा लगेगा”.
पल्लवी जी सवाल उठाती
हैं कि क्या हम बच्चें अपनी सुख सुविधा के लिए ही सिर्फ लातें हैं? क्या वे हमारे
नौकर या ऑटोमेशन टू बी प्रोग्राम्ड हैं? उनका कहना बिलकुल जायज है कि हर व्यक्ति
का नितांत अलग व्यक्तित्व होता है. कोई जीवन भर आपसे जुड़ा रहेगा तो कोई नहीं. क्या
पता कल को आपके बच्चें इतना समर्थ ही न हो कि देख भाल कर सकें. क्या पता कल को वे
किसी बीमारी या मुसीबत के मारे काम ही न कर सकें. उनके कहने का तात्पर्य है कि
बच्चों पर निर्भरता आखिर रखें ही क्यूँ.
पूनम अहमद जी का कहना
भी बिलकुल सही है कि पहले संयुक्त परिवार होतें थें तो बच्चों का जाना खलता नहीं
था. आज कल माँ-बाप पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगतें हैं कि
बच्चें अपनी दुनिया में एक दिन अपने भविष्य के लिए जायेंगे ही.
मुझे भी यही लगता है कि संयुक्त परिवारों का
विघटन और एकल परिवारों का चलन ने ही इस एकाकीपन को जन्म दिया है. पहले बच्चें भी
अधिक होतें थें, भाई बहन मिल कर माँ बाप के बुढ़ापे को पार लगा लेतें थे. एक दो अगर
विदेश चले भी गएँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता था. अब जब एक या दो ही बच्चें हैं तो हर
बार समीकरण सही नहीं हो पता है जीवन को सुरक्षित रखने का.
पुणे में रहने वाली
जोयश्री जी कहतीं हैं कि अगर बच्चों को मन पसंद करियर चुनने और जीने का अधिकार है
तो सीनियर सिटीजन्स को भी इज्जत के साथ जीने और शांति पूर्वक मरने का हक है. वे दो
टूक शब्दों में कहती हैं यदि बच्चें देखभाल करने में खुद को असमर्थ पातें हैं तो
उन्हें माता पिता से भी किसी भी तरह के विरासत की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए.
एक खबर के साथ शुरू
हुई हमारी इस लाइव डिस्कशन को हमने दीपान्विता रॉय बनर्जी कि इस सार ग्रभित
सुझावों से विराम दिया,
“वास्तविकता के
मद्देनजर अगर माता पिता बच्चों को बिना उम्मीद पाले, बिना अपने किये का हिसाब गिनाये कई स्मार्ट विकल्पों पर ध्यान दें मसलन
वृद्धाश्रम या सामाजिक सरोकार वाले आश्रम तो बखूबी अपनी जिंदगी किसी पर थोपे रखने
के एहसास से बचा कर अपने ही हमउम्र लोगों
के साथ हंसते मुस्कुराते कुछ नया करने सीखने और साझा करते जिंदगी बिता सकते हैं। जब
दूसरों को सुधारने की गुंजाइश नहीं रहती है तो खुद को कई बातें सहज स्वीकार करनी
होती है। बच्चों को उनके करियर और विकास से दूर तो नही कर सकते। दूसरी बात पहले
बच्चे अक्सर माता पिता के साथ ही रह जाते थे चाहे नौकरी हो या पारिवारिक व्यवसाय
पर अब करियर के विकल्प के रूप में पूरा आसमान उनका है। माँ पिता कब तक उनके साथ
चलें। उन्हें तो थमना ही है एक जगह। बेहतर हो परिवर्तन को हृदय से स्वीकारें और यह
युवा होती पीढ़ी के हम माँ पिता अभी से इसके लिए खुद को तैयार कर लें.
प्रकाशित व् नामित
सभी लेखिकाओं के विचारों से सज्जित








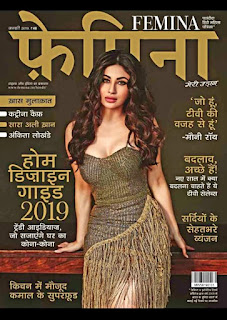

वाह बेहद उम्दा
ReplyDeleteधन्यवाद
Delete